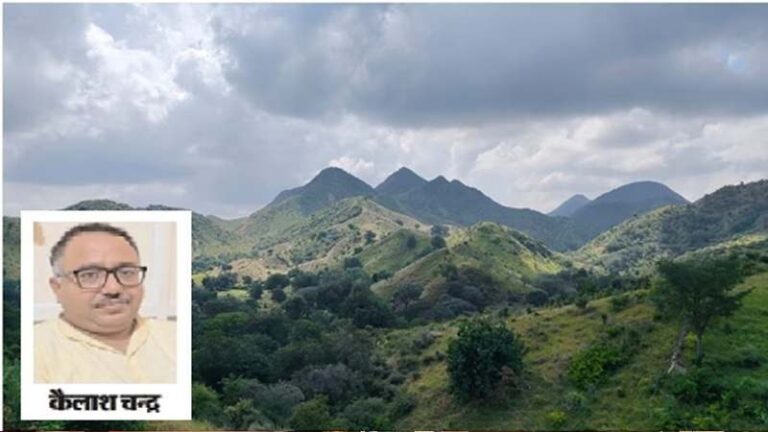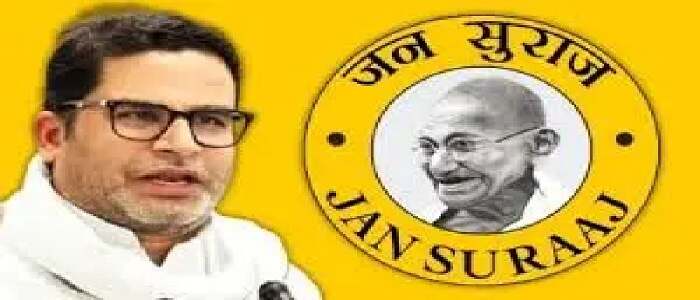डॉ. मेनका त्रिपाठी
कुम्हारो का गाँव सम्भलकर चलने वालों का गाँव था—चारों ओर मिट्टी की पगडन्डियाँ, बिखरे आम-जामुन के पेड़, और दूर से दिखता एक विशाल घर, जिसके चौड़े दरवाज़े और ऊँची देहरी मानो किसी ज़मींदारी की बू जैसी लगती थी। इसी घर में रहता था सीतो सरदार—लम्बा, गठीला, घनी मूँछों को ऊपर की ओर तिरछा खींच कर रखने वाला आदमी। गाँव में उसका इतना रौब कि कोई सामने पड़ जाए तो नज़रें नीची कर ले। दो शादियाँ की उसने—पहले कमलो, फिर केशो।
दोनों पत्नियाँ—पर दोनों ही बाँझ, औरतों की नज़र में अभागिन, मर्दों की नज़र में अपूर्ण।
कमलो की आँखों में सदैव एक स्थिर धैर्य रहता था। साँवली, पतली देह, सूती साड़ी का पल्लू हमेशा सिर पर।
केशो उससे गोरी, भरी देह की, पर चेहरे पर ऐसी थकान कि उम्र अपनी सीमा से कई कदम आगे दिखती थी।
दोनों सौतन थीं, पर दुख जब एक जैसा हो तो औरतें सौतन नहीं रहतीं, बहनें बन जाती हैं।
सीतो सरदार के मरते ही गाँव की फुसफुसाहटें तेज़ हो गईं—
“मनहूस औरतें हैं।”
“दोनों ने खानदान डुबा दिया।”
“अब क्या ही करेंगी? कौन सहारा?”
लेकिन कमलो और केशो इस अपमान की आदी थीं।
वे चुप थीं—चुप… और यही चुप्पी दुनिया को चुभने लगी।
सीतो के रहते घर में शान थी—पितरों से मिले खेत, अनाज के कोठार, दाल-चावल का भंडार, दो बैल, एक पुरानी बैलगाड़ी।
पर विधवा होते ही समाज का दूसरा चेहरा सामने आया।
जिसके हाथ जो लगा, ले गया।
सीतो के छोटे भाई ने खेत अपने नाम लिखवा लिए।
मल्लू बनिया ने उधारी का झूठा हिसाब थमा दिया।
कुछ और लोग आए और घर के कोठार में हाथ साफ कर गए।
गाँव भर में कोई था नहीं जो दो विधवाओं के लिए खड़ा होता।
क्योंकि भले घर की बहू-बेटियाँ बाहर नहीं निकलतीं।
और उनकी यही मर्यादा उनकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गई।
धीरे-धीरे घर खाली होता गया—
भंडार ग़ायब, कोठार का ताला टूटा हुआ, दाल-चावल खत्म, लकड़ियाँ खत्म, यहाँ तक कि बर्तन भी आधे रह गए।
रोज़ शाम दोनों चूल्हा जलातीं।
गाँव वाले देखते—
धुआँ उठता है…
आवाज़ें आती हैं…
“जिज्जी, आलू उबल गए होंगे।”
“अरे, आटा ज़्यादा मत मांडियो—रोज़ वैसा ही करती हो तुम!”
लोग कहते—
“देखो इन्हें! खाते ऐसे हैं जैसे अभी भी सरदार घर में जिन्दा हो!”
कानाफूसी बढ़ती गई—
“माल दबाकर बैठी हैं।”
“ये दो विधवाएँ खूब चैन से खाती हैं।”
पर किसी ने यह नहीं देखा कि बरतन में आलू नहीं, पत्थर उबलते थे।
हाँ—पत्थर।
कमलो डबडबाई आँखों से पत्थर उठाती, देगची में डालती और ढक्कन कस देती।
चूल्हे की आग पर पानी उबलता—
ठक… ठक… ठक…
पत्थरों की टकराहट की आवाज़ से लगता मानो घर में खाना बन रहा हो।
केशो उसी के साथ वही संवाद दोहराती—
“जिज्जी, आलू उबल गए होंगे।”
फिर हँस पड़ती—एक टूटी, दर्द भरी हँसी।
कभी रोने लगती—
“आज तो तरकारी भी बना लेती… अगर होता तो…”
गाँववालों की नज़र में यह खाना पकने की आवाज़ थी—
पर कालू जैसे चोर की आँख में यह दुर्भाग्य का नंगा नाच था।
कालू—गाँव का कुख्यात चोर—सोच रहा था कि दो बुढ़िया माल दबाकर बैठी हैं।
एक दिन भूसे में छुपकर उसने घर की झोपड़ी से आती आवाज़ें सुनीं।
जो वो देख रहा था—उसने उसकी आँखें झुका दीं।
दोनों औरतें एक दूसरे का सहारा बनी बैठी थीं।
कमलो चूल्हे में लकड़ी डालती, केशो अपनी साड़ी का कोना दाँतों से दबाकर आँसू छुपाती।
दोनों बुज़ुर्ग, झुर्रीदार आँखें, थकी देहें—पर माथे पर शान की वह लकीर अब भी जिंदा थी।
क्योंकि वे दुनिया को दिखाना नहीं चाहती थीं कि
उनके घर में अब कुछ नहीं है।
नमक नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं।
पर रसूख की परम्परा उन्हें मजबूर करती थी कि चूल्हा दोनों वक़्त जले।
भले वह चूल्हा पत्थर उबालकर ही क्यों न चलता हो।
रात को दोनों पत्थरों की खनखनाहट सुनकर पेट पर हाथ फेरतीं—
“जिज्जी, आज भूख ज्यादा लगी है…”
“सो जा बहिनी, भूख नींद में छिप जाती है…”
उनकी उम्र पचास पार हो चुकी थी, पर जीवन का बोझ सौ बरस का था।
कमलो के सफेद बालों में धूल चिपकी रहती, केशो के पाँव में दरारें थीं—ऐसी कि उनमें दर्द उतर आता।
धीरे-धीरे कालू को सच्चाई समझ में आने लगी—
यह घर तो लुट चुका है।
जो बचा था, वह दो स्त्रियों की इज्ज़त और खामोश आबरू थी।
पर भूख इंसान को कितनी देर तक रोक सकती है?
उनके शरीर ढांचे जैसे रह गए—बिना रोए आँसू बहाते हुए।
कालू का दिल फिर भी चोर का ही था—
वह चुपचाप झोपड़ी में घुसा।
उसे उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा—पर उसे केवल
एक खाली बर्तन, कुछ पत्थर, और दोनों स्त्रियों की सूजन भरी आँखें दिखीं।
उसने अपने जीवन में इतनी दयनीय मनोरंजक—और दर्दनाक—स्थिति कभी नहीं देखी थी।
दो विधवाएँ, जो सौतन होकर भी सगी हो गई थीं, भूखे पेट अपनी मरती हुई शान को बचाने के लिए पत्थर उबालती थीं—
रसूख की आँच में खुद को जलाती हुई।
कालू बगैर कुछ लिए भाग गया।
उसे लगा जैसे उसने उनके दर्द में झाँककर कोई पाप कर लिया हो।
और दोनों?
अगली शाम फिर कमलो बोली—
“जिज्जी, पानी चढ़ा दूँ?”
केशो बोली—
“हाँ बहिनी… आज थोड़े बड़े पत्थर डालना… पेट भर जाएगा…”
और चूल्हा जल उठा—
एक बार फिर।
एक रस्म की तरह।
एक मरते हुए अभिमान की तरह।
कमलो और केशो की भूख नहीं मरती थी—
उनकी शान मर रही थी, पर आँच अभी भी बची थी।
और यही थी—
रसूख की आँच
लेखक परिचय
डॉ. मेनका त्रिपाठी हिंदी साहित्य की समर्पित शिक्षिका, प्रख्यात लेखिका और प्रतिष्ठित विद्वान हैं। बीस वर्षों से अधिक के अध्यापन अनुभव के साथ उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति का गहन बोध कराया, बल्कि साहित्यिक सृजन और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट प्राप्त करने के उपरांत उनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हुईं, एक पत्रिका का संपादन किया और 32 से अधिक शोध-पत्र, आलेख और कविताएँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं।
उन्होंने 40 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध प्रस्तुतियाँ दी हैं और मॉरीशस, फिजी, कजाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन एवं साहित्यिक आयोजनों में भाग लेकर हिंदी का गौरव बढ़ाया है।
उनकी विद्वत्ता को मिलेनियम की महिला, ग्लोबल आइकॉन अवॉर्ड, मुंशी प्रेमचंद सम्मान, ज्ञान भारती राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, सर्वोत्तम शिक्षक पुरस्कार और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन लाइफटाइम इंटरनेशनल अवॉर्ड सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
साहित्य और शिक्षा के साथ-साथ वे बॉलीवुड में पटकथा, गीत, संवाद लेखन मीडिया और वृत्तकथा निर्माण के माध्यम से भी सक्रिय हैं। उनके “संवाद चैनल” (YouTube) के जरिए नियमित रूप से कई प्रेरक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिनसे वे हिंदी सेवा समूह और समाज की सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ी हुई हैं।