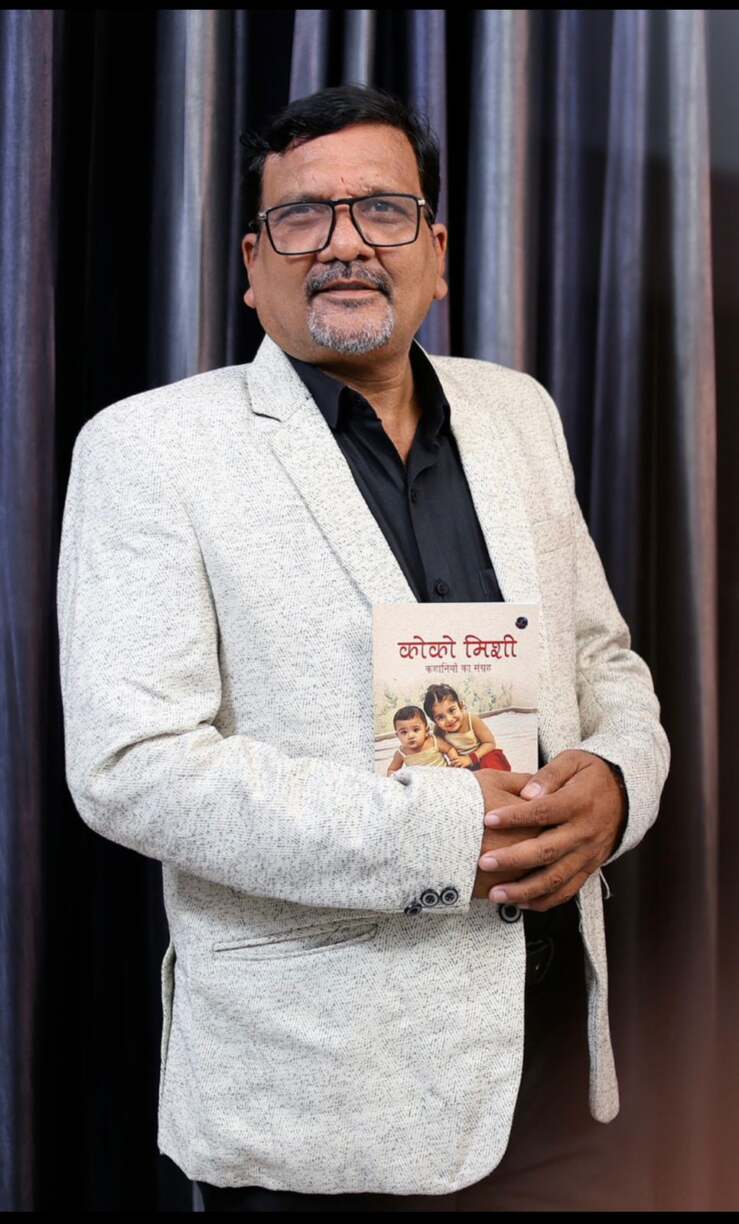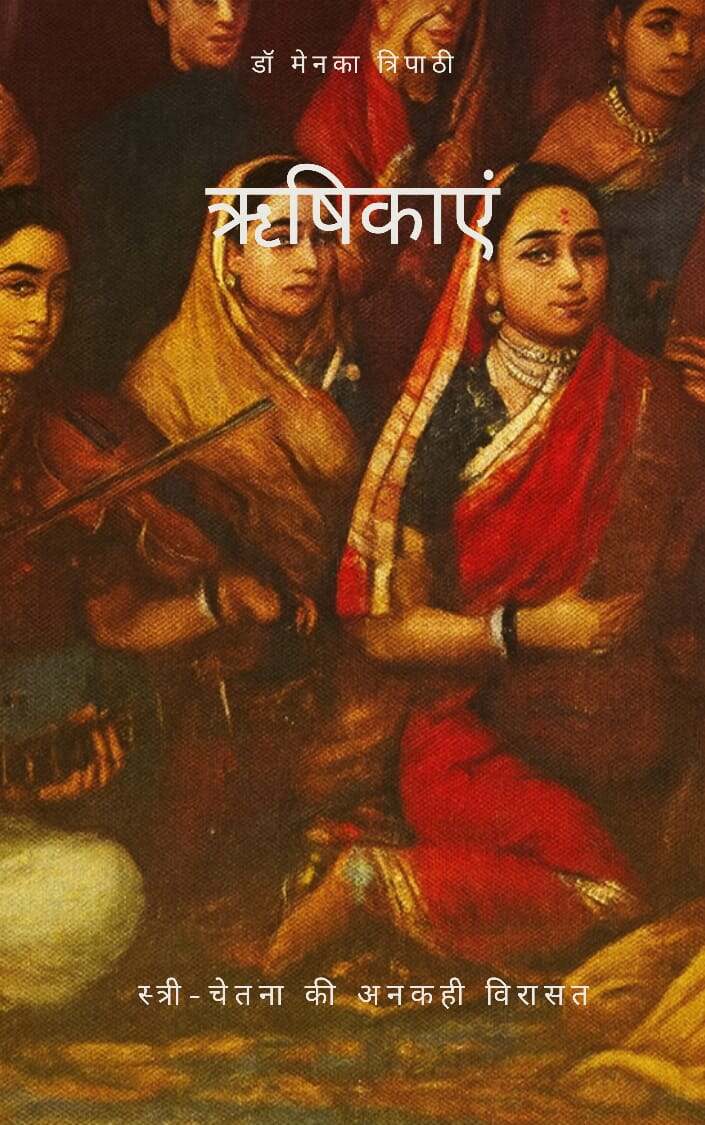
भूमिका / प्रस्तावना
मैं उस पीढ़ी की स्त्री हूँ, जिसने अपनी पाठशाला के दिनों में “हमारे पूर्वज” नाम की एक पतली-सी किताब में पहली बार सभ्यता के प्रकाश को छुआ था। लकड़ी की बेंचों पर झूलते-दुलकते हम बच्चे भले ही उन पंक्तियों को खेल-खेल में पढ़ते थे, पर आज समझ आता है कि दरअसल वही पन्ने हमारी आत्मा में अपनी जड़ें डाल रहे थे। उस किताब में केवल पुरुष नायक नहीं थे—वहाँ ऋषियाँ भी थीं, तपस्विनियाँ भी थीं, बुद्धि, साहस और संयम से भरी स्त्रियाँ भी थीं। वे कहानियाँ मेरे भीतर इतनी गहरी उतरीं कि उन्होंने मेरी चेतना का ढाँचा ही बदल दिया।
पर समय के साथ एक दुखद परिवर्तन आया।
दुनिया भागती चली गई, किताबें चमकदार हो गईं, पाठ्यक्रम बदल गए, और हमारी सभ्यता की स्त्रियाँ—धीरे-धीरे पन्नों से ओझल होने लगीं। आज जब मैं युवा पीढ़ी से पूछती हूँ—“क्या तुम गार्गी को जानते हो?” मुझे केवल रिक्त चेहरों का सामना करना पड़ता है। “मैत्रेयी? कात्यायनी? लोपामुद्रा? विश्ववारा? अपाला?”—ये नाम उनके लिए उतने ही अनसुने हैं जितना किसी पुराने काल की गूँज।
यह विस्मृति मुझे भीतर से तकलीफ़ देती है।
क्योंकि जिस समाज की आत्मा अपनी स्त्रियों को भूल जाए, वह अपने भविष्य का मार्गदर्शन किससे लेगा?
आधुनिक स्त्री-विमर्श ने निश्चित रूप से आवाज़ उठाई है, विद्रोह जगाया है, प्रश्न खड़े किए हैं—पर कई बार उस विद्रोह के शोर ने स्त्री-शक्ति की मूल धुन को ढक भी दिया है। वह धुन जो ऋग्वैदिक ऋषिकाएँ गाती थीं—
शांति में शक्ति,
विवेक में विद्रोह,
करुणा में गहराई,
तप में तेज,
और धैर्य में क्रांति।
इस पुस्तक का पहला खण्ड उन दस ऋषिकाओं की पुनर्स्मृति है—
घोषा, अपाला, विश्ववारा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपामुद्रा, सुलभा, अरुंधति और अनुसूया।
ये केवल पात्र नहीं, वे स्त्री-चेतना के उज्ज्वल स्तंभ हैं।
इन ऋषिकाओं को जानना अपने भीतर की भूली हुई रोशनी को पहचानना है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पुस्तक को उस क्रम में पढ़ें जैसा मैंने रखा है।
पहले प्रकाश को पहचानिए—फिर छाया को।
पहले ऊँचाई को देखिए—फिर मानव दुर्बलताओं को।
पहले ऋषिकाओं को पढ़िए—फिर अनकही स्त्रियों को।
क्योंकि स्त्री-यात्रा केवल तेजस्विता की यात्रा नहीं है।
वह टूटने, बिखरने, गलत समझे जाने, गलत निर्णय लेने, और फिर भी आगे बढ़ने की यात्रा है।
जब मैंने पहले खण्ड की ऋषिकाओं को लिखा,
मेरे भीतर बार-बार यह आवाज़ आई—
“हर स्त्री में कोई न कोई ऋषिका अभी भी जीवित है,
बस उसे पहचानने की दृष्टि खो गई है।”
और इतने में ही मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई थी।
मेरे भीतर एक और रास्ता खुला—एक ऐसा रास्ता जिसे समाज ने छाया में ढकेल दिया था।
वे स्त्रियाँ जिनके नाम सुनकर लोग कन्नी काट लेते हैं,
जिन्हें परंपरा ने दोषी घोषित कर दिया,
जिनकी कहानी आधी सुनाई गई और आधी छुपा दी गई।
तभी मैंने दूसरा खण्ड लिखा—अनकही स्त्रियाँ।
यहाँ आएँगी कैकई—
जो केवल “कान की कच्ची” कहकर अपमानित कर दी गई,
जबकि उसके भीतर एक शूरवीरता, शक्ति और प्रेम की गहरी नदी बहती थी।
यहाँ आएगी रावण की दादी—जिसकी कथा किसी ने ठीक से सुनी ही नहीं।
मंदोदरी—जिसने राक्षसराज के घर में भी विवेक की लौ जलाए रखी।
कुब्जा—जिसे इतिहास ने केवल शरीर से आँका, पर जिसके भीतर मन का अपना ही संघर्ष था।
हिडिंबा—जिसे राक्षसी कहा गया, पर जिसने अपने वंश की रक्षा में अपना जीवन खपा दिया।
सची—इंद्र की पत्नी, जिसके हृदय में प्रेम भी था और insecurity भी।
रेणुका—जिसका गला उसके ही पुत्र ने काट दिया, और आज भी कितनी स्त्रियाँ उसी मानसिक वध से गुजरती हैं।
अहिल्या—जिसे बिना अपराध के पत्थर बना दिया गया, जैसे आज भी कई स्त्रियाँ मन से पत्थर हो जाती हैं।
और अंत में—
मैं, मेनका।
क्योंकि मेरा नाम जब लोग सुनते हैं तो वे केवल अप्सरा देखते हैं—
जबकि उसका वास्तविक अर्थ है—‘मन को एकाग्र करने वाली’।
मेरा नाम किसी प्रलोभन का नहीं, साधना का अर्थ रखता है।
मैंने यह पुस्तक इसलिए लिखी है कि मेरी पहचान मेरे नाम के मिथकों से नहीं,
मेरे शब्दों से बने।
मैं चाहती हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ते हुए अपने भीतर झाँकें—
कौन-सी ऋषिका आपके भीतर सोई है?
कौन-सी अनकही स्त्री आपके भीतर संघर्ष कर रही है?
कौन-सी छाया आपको परेशान करती है?
और कौन-सा प्रकाश आपको दिशा देता है?
क्योंकि सच बताऊँ—
कोई भी स्त्री केवल प्रकाश नहीं होती,
और कोई भी स्त्री केवल छाया नहीं होती।
हर स्त्री अपनी ही कहानी की जटिल, सुंदर, अधूरी और अलौकिक कविता है।
मैंने यह पुस्तक एक आईना बनाकर आपके सामने रख दिया है।
अब यह आप पर है कि आप उसमें कौन सा रूप पहचानती हैं—
ऋषिका, स्त्री, साधिका, योद्धा, छाया, या प्रकाश।
काश यह पुस्तक आपके मन के किसी कोने में एक नया दीप जला सके—
और आप स्वयं से यह कह सकें—
“मैं भी एक ऋषिका हूँ।
मैं भी अपनी कहानी की प्रकाश-रेखा हूँ।”