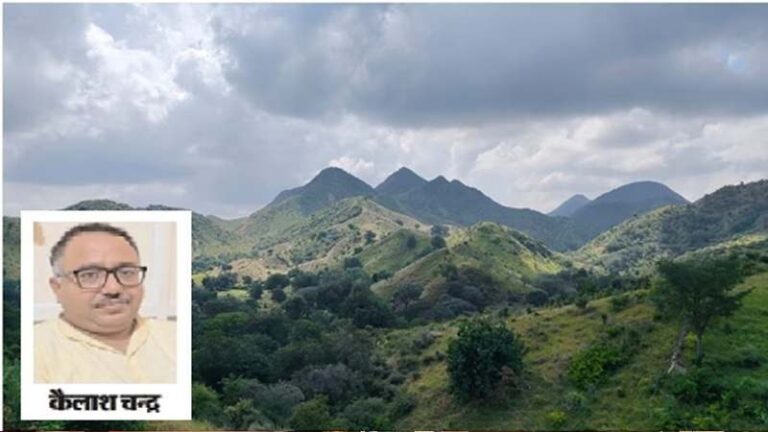एक स्त्री, कई सुबहें – कल्पना मनोरमा
कहानी
शॉपिंग से लौटते वक्त मैंने कलाई पर नज़र डाली। घड़ी दस बजा रही थी। सुबह जल्दी चाची के घर निकलना था। मैंने पति से डिनर बाहर खाने की गुजारिश की। मुस्कुराते हुए वे बोले—“अरे यार! तुम चिंता मत करो। मैं मदद करूँगा। साथ में कॉफी पिएँगे। ढेर सारी बातें… तुम्हारी शिकायत थोड़ी तो कम कर सकूँगा।”
कभी-कभी मीठे शब्द मन बाँध लेते हैं। मान लिया। घर आकर सामान अटैचियों में सहेजा और लग गई किचन में। पति को साबुत लहसुन के तड़के वाली उड़द दाल और बाजरे की रोटी खाना था। बिटिया सो चुकी थी—अच्छा था। उसके कपड़े बदलकर ठीक से सुला दिया। दाल उबलने चढ़ा कर खुद भी कपड़े बदल लिए। मैं देखती रही—खाना मेज़ पर लगाने तक जनाब मदद के लिए नहीं पहुँचे।
“आइए, खाना ठंडा हो रहा है।” मैंने कहा।
“प्लेटें लगा लो। बस अभी आया।” पति बोले।
मन खिन्न हो गया। उनकी किसी भी मज़ाक पर फिर हँसी नहीं आई।
‘थकान ज़्यादा है… सोने जा रहा हूँ’ कहते हुए वे भी सोने चले गए। थके न भी होते तो भी क्या साथ देते? खिसियाते हुए किचन साफ़ किया। बचा सामान बैग में जमाते-जमाते रात का एक बज गया। जब सोने गई तो साहब के खर्राटों से मन विचलित हो गया। क्या करूँ? पलट कर उनकी नाक दबा दी। आवाज़ थमी तो राहत मिली, मगर थकी आँखें भीग चलीं। पति की चिल्लाहट। जल्दी से सॉरी बोलकर करवट बदल ली। कुछ देर बाद गुस्से की गाँठ तो ढीली पड़ी—पर नींद नहीं आई। मोबाइल देखा। सुबह के पाँच बज रहे थे। बालकनी में जाकर बैठ गई। धुंधली-सी रोशनी फैल रही थी। उसी धुंधलके में माँ की आवाज़ जैसे भीतर कहीं गूँज उठी—“पराये घर न जाना होता तो कला को कच्ची नींद न जगाती…”
मुझे उनकी बातें कभी समझ नहीं आईं। कार्यों की लंबी सूची और पराए घर का डर। क्या सब माँओं को होता होगा? अगर जान पाती कि जीवन में इतना जागना पड़ेगा, तो शायद इंकार करना भी सीखती। किस्मत की दुहाई देते हुए रसोई की लाइट जला दी। कॉफी-कैटल का स्विच ऑन कर दिन का शुभारम्भ किया। कहवा की खुशबू नासापुटों को सहलाने लगी। किचन-टॉप पर अल्साई बैठी मैं, स्फूर्ति में भरकर जागने का प्रयास करने लगी। खिड़की से मुँह सटाकर देखा—क्षितिज पर एक-दो पंछी आसमान बुहार रहे थे।
बस रात का हाथ वहीं से छूटा तो छूटता चला गया।
“कला..! कहाँ हो यार…?” पति ने बुलाया नहीं—एक गायकी आलाप ली।
“जी..! कहो…मैं यहीं हूँ।”
“नितेश की शादी में जाना भी है… या बस सोती रहोगी..?”
“उठोगे तो देख सकोगे।”
कहा नहीं, सोचा। उन्हें अचानक ज़िम्मेदारी का बोध हो आया था। मेरे भाग्य में सोना लिखा ही कहाँ…? गुस्सा साँसों में उतर आया। मन की मलामत दबाते हुए बोली—“आप सोच लो, मैं तो तैयार हूँ…!”
“अबे यहाँ तो आओ…! नाराज़ क्यों होती हो।”
“सुबह…? दोपहर होने में बस आधे घंटे की कमी है। सोये रहो। शादियाँ तो होती ही रहती हैं।”
रात के गुस्से में खिड़की के पर्दे खींच दिए गए। एकाएक उजाला उन्हें तकलीफ़ से भर गया।
“पर्दे बंद करो न।”
न मानने का मतलब—झगड़ा। सो चुपचाप कर दिए।
“अब बोल भी दो, क्या चाहिए।” कुढ़न दबाते हुए मैंने कहा।
“अच्छा सुनो—एक किस, एक गिलास गुनगुना पानी, स्लीपर, शेविंग-किट दे दो। मोबाइल भी चार्जिंग पर डाल देना। और तैयार हो जाओ। तुम स्त्रियों को घंटों चाहिए…”
उन्होंने इतनी नज़ाकत से कहा, जैसे रूम सर्विस उनके आगे खड़ी हो। कहाँ वे विनम्र औरतें, और कहाँ मैं। सहजता से नहीं ले सकी। ब्याहता हूकें चेहरे पर पसर गईं। भीतर एक घुटा-सा स्वर उठा—इन्हीं कारणों से शादियों में काठ पैदा होने लगता है।
“क्या कहा?”
“कुछ नहीं। अपनी सुनो।”
“ठीक है। जब नाश्ता टेबल पर लग जाए तो बता देना।”
“नाश्ता… या लंच?” मैंने कहा।
“तुम जो समझ लो। और मेरे अंडरगार्मेंट्स बाथरूम में रख देना। मैं नहाने जा रहा हूँ।”
कामुक अंगड़ाई लेते हुए शीशे में खुद को निहारा—“कला, यू आर सो हॉट!”
पसीने से तर मैं, आनंद में डूबे आप—फिर भी हॉट?
मैंने उन्हें उसी नज़र से देखा जिसमें खेद और खीझ दोनों थे। मगर उनकी बला से।
“जो माँगना है, कहो।”
“जो माँगना है, माँग लूँ? छोड़ो भी… बाकी मैं खुद देख लूँगा।”
आँख मारते हुए वे निकल गए। मैं बिना प्रतिउत्तर बेबी के गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन तक पहुँची ही थी कि फिर आवाज़ आई—“कला, जूते-मौजों के साथ मेरे कपड़े भी देख लेना। आयरन की ज़रूरत हो तो कर देना। और ये क्या—मेड की छुट्टी कर दी? ये गलत किया, मेरी जान।”
उन्होंने मुझे खुश करने की उतनी ही जहमत उठाई, जितनी च्विंगम पर चिपकी मिठास। “शादी जब तक समझदार नहीं बनती, पति की चालाकियाँ पढ़ी-लिखी बीवी को भी समझ नहीं आतीं। सिर धुनते-धुनते स्त्री पत्थर बन जाती है।”
“देवी जी, क्या बड़बड़ा रही हो?”
पास से गुज़रते हुए पति बोले। क्या कहती। उनका माँगा उन्हें मिल चुका था। मुझे क्या चाहिए—इससे न उन्हें मतलब था, न मैंने खुद को कभी महत्व दिया था। न अपने लिए, न बेबी के लिए कुछ तय किया था। क्या पहनना है, कैसा लगना है—कुछ भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ बस लुढ़क रही थी।
सुबह से फूलवाला, दूधवाला, अख़बारवाला—न जाने कितने ‘वालों’ को समझा चुकी थी कि आज के बाद कब लौटना है। क्या ये काम गिनाने लायक थे? पति के हिसाब से नहीं। तो फिर क्या कहना।
काम की आख़िरी खेप समेटी। तब कहीं जाकर ढाई बजे साड़ी पहनने का नंबर आया।
“घर से जल्दी निकलेंगे। कहा था न! अब हो गई न देर। ये शादी घर की है—थोड़ा तो मेरे बारे में सोचा होता। नीचे आओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। और सुनो—ताले ठीक से लगाना।”
उनकी बात उन्हीं के पास छोड़कर मैंने कहा—“ठीक है। बेबी को सैंडिल पहनाकर साथ ले जाओ।”
“ये भी काम मुझे करना पड़ेगा? वेरी गुड!”
“फिर छोड़ो…” मैं बोली।
“अब लाओ भी…।” उन्होंने बेबी को सोफे पर दचक लिया। आदमखोर अहम वातावरण में झन्न से उभरा और बालू में पड़े पानी की तरह बिला गया। मन तो हुआ साड़ी खोलकर फेंक दूँ और सो जाऊँ।
“तुम इतनी बड़ी हो गई हो… फिर भी ‘चप्पल’ पहननी नहीं आती? जैसी माँ, वैसी बेटी!”
“पापा, ये तप्पल नहीं है…।” सुबकते हुए बेबी मुझे देखने लगी। उसके चेहरे से टपकती निरीहता मेरा सीना चाक कर गई। साड़ी पहनना बीच में रोक दिया। कहा—“आप जाएँ! मैं पहना लूँगी।”
सुनते ही सैंडिल बच्ची को पकड़ाते, कानी उँगली में चाबी घुमाते हुए बंदा फुर्र। थोड़ी देर बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। पति सीटियाँ बजा रहा था। बेबी किलक रही थी। मैं उबले भात-सी सीट पर पसरी फुटपाथ की अफ़रातफरी देख रही थी। कुछ अच्छा देखने की चाहत में आँखें सड़क के किनारे—खाल गाँठते मोची, बोहनी को तरसते ठेली वालों पर जा टिकीं। मेरे भीतर उदास साँसों की बाँसुरी बज उठी। नज़रें ऊपर उठीं तो धूल के गुबार में लाल गाल लिए सूरज पीठ फेरने को आतुर दिखा। उदासी घटने की जगह बढ़ गई। बहुत ढूँढने पर भी स्निग्धता नहीं मिली तो लगा—मैं ही बहुत थक चुकी हूँ। स्वयं से चिढ़कर आँखें मींच लीं। मैं मौन रहना चाहती थी, मगर बिटिया प्रश्न करने के मूड में आ चुकी थी। बावजूद इसके होंठ शिथिल होकर एक-दूसरे से चिपक गए। आँखों के किनारे चिपचिपे होने लगे। रूमाल से आँखें पोंछी—पर कुछ असर नहीं हुआ। छोड़ दिया। जिस बात को मैंने छोड़ा, उसी को चुटकी लेते हुए पति ने उठा लिया—“क्या हाल बना रखा है! कभी तो ‘रोमांटिक फेस’ बना लिया करो। दुनिया में औरतें पॉपकॉर्न की तरह फूटती रहती हैं। एक तुम हो—लुटे-पिटे बनिये की तरह, मसालों में डूबी। बुझी। ठंडी औरत।”
“कौन है ये आदमी…?” मेरे भीतर की स्त्री ने पूछा। मैं कुछ बोलती—पति बोले, “बनिये से ध्यान आया… तुमने सिलेंडर से गैस बंद की थी?”
“……”
“बोलती क्यों नहीं? बड़ी बालकनी का ताला…? तुम्हें मज़ाक लग रहा होगा। मगर अभी एक हफ़्ते पहले शर्मा-परिवार शादी में गया था। लौटा तो घर साफ़ मिला।”
पति लगभग स्टेयरिंग पर झुक आए थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। थकान के ऊपर अब भय फूट पड़ा। मुझे अपनी कार्यगुजरियों पर शक होने लगा। गैस की नॉब बंद करने का सूत्र पकड़ से बाहर ही रहा। घर से दूर निकल चुकी थी। लौटने का मतलब चाची का रूठ जाना—फिर भी लौटकर देख लेना चाहती थी।
मैंने कहा—“गाड़ी घुमा लो। पाँच मिनट देर से पहुँचे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा घर राख हो जाएगा।”
मैंने कहा—पर सुना नहीं गया। कामों की सूची याद करती रही। हल न निकला तो प्रार्थनाएँ शुरू हो गईं।
“क्या बुदबुदा रही हो? खुलकर बोलो… तुम्हारा कोई दोष नहीं। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी लापरवाही हम ही झेलेंगे—पति जो ठहरे!”
गाड़ी चलाते हुए उन्होंने बाईं कोहनी मेरी छाती में गड़ा दी। मैं दर्द से कराह उठी।
“आगे देखो… वरना—” चोट सहलाते हुए कहा।
“वरना क्या?”
“शहर में आज कितनी शादियाँ हैं? हर दूसरी कार पर ‘फलाने परिणय ढिकाने’ के पोस्टर लगे हैं।” बात बदलने की गरज से कहा। क्योंकि मेरे आँसू एक बार छलके तो घंटों रुकते नहीं।
“क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? सब मेरे जैसे नहीं होते—शादीशुदा, कुँवारे।”
“मुझे क्यों होगी जलन? कुँवारे तुम हो सकते हो, मैं तो हरगिज़ नहीं।”
“बोलते-से परिणय पोस्टर और…।”
मैंने आँखें बंद कर लीं। वे चिढ़ गए। गाड़ी की रफ़्तार से महसूस हुआ। पल-भर की देरी से फूलों से सजी एक लाल कार शीशा खरोंच देती—यदि महोदय बचा न लेते।
“देखा? क्या कमाल का पोस्टर था—‘सुकेश परिणय सुनयना!’”
मेरी साँसें थमी ही नहीं थीं कि पति ने मेरी टाँग पर गहरी चुटकी काट ली। झुँझलाकर पारा चढ़ गया, आँखें भर आईं।
“कितने भी पोस्टर बोलते-से क्यों न हों… स्त्री की बोलती बंद करना सब जानते हैं। कायदे से इन्हें ‘परिणय पोस्टर’ नहीं—‘दमघोटूं पोस्टर’ कहना चाहिए।” क्षुब्ध मुस्कान होंठों को छू गई, जो पति को ज़हर लगी।
“कुछ कहा?”
“मेरे पास कहने को बचा ही क्या है? वैसे भी युग बीते हमारे परिणय को। गाड़ी ठीक से चलाओ—सही-सलामत घर भी लौटना है।”
“युग तो नहीं… तुम्हारा हुलिया ज़रूर!” कहते हुए उन्होंने गाड़ी पाँचवें गियर में डाल दी। लगा—इस आदमी के चक्कर में रोडरेज में मुझे भी धर लिया जाएगा। ऊपर से अपनी हाय-तौबा में बेबी को जगाए रखना भूल गई थी। पीछे की सीट खाली होते हुए भी बच्चे को गोद में लिए सफ़र तय करती मध्यमवर्गीय माँओं की तरह, मैं थके तन-मन से अपनी भावनाएँ समेटने लगी।
ससुराल की ओर मुड़ने वाले रास्ते पर लगा होर्डिंग—‘कानपुर की शान पान पराग’ दिख गया। मैं सिर ढकने की जुगाड़ में थी, तभी पति बोले—“सिर तो ठीक से ओढ़ लो, मैडम! हम घर पहुँचने वाले हैं। वैसे तो कोई रोक-टोक है ही नहीं।”
मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। सुबह से शाम तक खिदमत—और ये बोली।
“ओढ़ क्या लें…? पल्ले पर बेबी सोई है।”
“ओहो…! तो क्या पल्लू भी मैं ठीक करूँगा?”
मैंने घूमकर उन्हें देखा—“जैसे, फूलों के पालने से उठाकर गाड़ी तक गोद में तुम ही लाए…”
कहा नहीं। कसमसाकर माथे तक घूँघट खींच लिया। दो-चार दुकानें छोड़कर गाड़ी घर के सामने खड़ी हो गई। रंगीन बल्बों की लड़ियाँ, आम-पत्तों की बंदनवार से घर सजा था।
“ये पपीता जैसा चेहरा लटका कर मत रखो। थोड़ा हँसमुख-सा सुधार कर लो। सामान गाड़ी में छोड़ दो। बेबी को लिए जाओ।”
उन्होंने फ़र्ज़-अदायगी की मिसाल पेश की। लेकिन सोते हुए बच्चे को लेकर चलना आसान नहीं था। ऊपर से मेरा एक पाँव सुन्न हो चुका था। मैं बेबी के साथ पाँव को जगाने लगी।
“अच्छा ऐसा है! हम तुम्हारे नौकर तो हैं नहीं… जल्दी से बाहर निकलो। चाचाजी क्या सोचेंगे? मैं तो बिल्कुल बीवी का गुलाम बन चुका हूँ।”
“चाचाजी अन्तर्यामी हैं… तो ये भी जान लेंगे—गुलाम आप नहीं, मैं बन चुकी हूँ।”
बोलकर मैं गाड़ी से उतरने लगी। पाँच मिनट तक पाँव पटकने के बाद—मैं चल पाई।
बेबी के लिए मैं कृतज्ञ थी। लेकर घर पहुँची। शादी की तैयारियाँ पुरज़ोर चल रही थीं—मंडप में तेल, हल्दी-अक्षत, आल्ता। कहीं किसी के पति अपना सूटकेस माँग रहे थे।
इसका मतलब… मैं ही अकेली नहीं….? अनकहा संतोष मन में उभरा। इंदौर वाली बुआ चाय के लिए रट लगाए थीं—“अरे कोई चाय पिया दो। राम जाने मायके की देहरी फिर चढ़े को मिले कि नाहीं…”
मैं देर से पहुँचने का अपराध-बोध समेटे कहीं कोने में बैठकर नई-पुरानी होना चाहती थी। अधसोई बिटिया कंधे पर लटकाए चप्पल छिपा ही रही थी कि बुआ की नज़र पड़ गई।
“हाय राम! धीरज की बहू को देखो तनी—हाथ में दीया लेकर आई है।”
मैं अपराधी नज़रों से सबकी ओर देखने लगी। कोई मुस्कुरा दे, तो मैं भी हँसकर जश्न में शामिल हो जाऊँ।
“लो जी…! भाभीजी आ गईं।”
नितेश मंडप से उठकर आया। उसके हंगामे में शायद बुआ की चाय में एक कप मेरा भी जुड़ गया होगा। थोड़ी देर में महराजिन चाय-नाश्ता ले आई।
उस रात मन ज़्यादा खुश न हो सका। सब सो गए, मगर मुझे नींद नहीं आई। बीता दिन के मलाल में मन मथता रहा।
सुबह घर में अलग उत्साह था। बारात जानी थी। बूढ़ी औरतें जवान हो चली थीं। दोपहर तक घर की महिलाएँ चटख मेकअप और नए परिधानों में सज गईं। मेरी बिटिया नए चेहरों से घबरा रही थी—गोद से उतरी ही नहीं। इसलिए मैंने री-फ्रेश होना टाल दिया और आँगन में दरी पर जाकर बैठ गई।
“चटक मेक-अप में कोई-कोई स्त्री कितनी सुंदर लगती है… दिन के उजाले में।” मेघा से यूँ ही कह दिया।
“अपनी-अपनी चॉइस है, भाभी। बट आई डोंट लाइक एनी मेक-अप। भाभी, आपने एम.ए. का फ़ॉर्म भरा?” उसने कंधा सहलाया—दुखती रग पर हाथ धर दिया।
“अभी तो बस सोचा ही है…”
मैं उसके चेहरे को देखने लगी। इस बार वह और भी गंभीर, और सुंदर लगी—खादी का इंग्लिश ग्रीन कुर्ता, नीली जींस, आँखों में अपने होने की चमक। सुबह से पहली बार कुछ अच्छा लगा। मेरी नज़र पति से टकराई। इशारे हुए—साड़ी बदलने के। मैं जानबूझकर दूसरी ओर देखने लगी। वे फिर इशारे करने लगे। अजीब ज़बरदस्ती थी। फिर भी मैंने साड़ी की सलवटें सीधी कीं, पल्ला सँवारा—उठी नहीं। पति के प्रति यह मेरा मौन, किन्तु खुला और पहला प्रतिकार था।
“और सुनाइए भाभी…”
“मैं… मेरा…” ज़बान लड़खड़ा गई। तभी आवाज़ आई—“कला, हरिअप।”
मेघा ने पूछा—“भाभी, आपको साड़ी बदलनी है?”
मैंने सिर हिला दिया—नहीं।
“देन जस्ट इग्नोर एंड एन्जॉय।”
मैं चकित थी। इग्नोर…? माँ ने तो सिखाया था—पति की अनुगामिनी बने रहना।
“कला…! सुना नहीं?”
रिश्तेदारों से घिरे बेबी के पापा पूरे रुआब में खड़े थे। लड़ने की जगह मौन धर लेना, मैंने पिता से सीखा था।
“क्या है धीरज भाई! लीव इट यार!” मेघा ने भाई को बाहर की ओर धकेला—“भाभी इन्हीं कपड़ों में कम्फ़र्ट महसूस कर रही हैं तो रहने दो। अगर साड़ी दिखाना इतना ज़रूरी है, तो आप ही पहन लो।” मेघा को यूँ कहते देखकर मेरी धड़कनें अस्थिर हो गईं। लगा बेबी के पापा हंगामा न मचा दें। मगर उनकी ओर से नज़र हटकर मेघा को देखने लगी। आत्मचेतना से भरी आवाज़। मेरे सिर का बोझ उतर सा गया। आँखों में ललछौंहीं शाम झूम उठी।
“ऊबते-चूबते हृदय में सागर जैसी प्रशांति!”
मैंने आँखें मूँद लीं। पति पास में खड़े थे। खड़े रहे। उनकी परछाईं का दबाव बराबर मुझे महसूस हो रहा था। मेघा ने बेबी को मेरी गोद से उठाया। झटके से मेरी आँख खुल गई। मैंने मंडप के नीचे बैठे नितेश को देखा। कामायनी गमक से घर का माहौल गमक रहा था। नितेश का चेहरा भी…
“मुझे इतना खुशनुमा लग कैसे सकता है..? लेकिन लग तो रहा था। सच्चाई को झुठला नहीं सकी…।”
मैंने पति को देखा। वे बाहर की ओर जा रहे थे—बीवी से पहली बार हारे हुए। चाची की भर्राई आवाज आई—“धीरज की दुल्हिन! कहाँ हो..?”
मैं अपना दुःख, खिसियाहट, मलाल झटककर उठने लगी। मेघा ने नहीं उठने दिया।
“मम्मा! आप तो नाम से पुकार सकती हो…? इतना प्यारा नाम है भाभी का!”
“अरे बिटिया! अपने यहाँ बहुरियाँ पति के नाम से ही बुलाई जाती हैं।”
“आप ये रिवाज बदलो मम्मा..!”
“अच्छा ठीक है… कला, बहुरिया आओ? नितेश की आँखें आँजो… वैसे ही देर हो चुकी है।”
चाची ने मुस्कुराते हुए काजल की डिबिया मुझे पकड़ा दी। पहले मन हुआ कि चाची के गले लग जाऊँ। फिर लगा—नितेश से पहले मेघा की आँखों में काजल की महीन रेखा खींच दूँ। “स्त्री की दृढ़ता भरी कजरारी आँखें!”
मेरे भीतर की स्त्री अब तक हल्की हो चुकी थी। उसने एकाएक उजाले की ओर छलाँग लगा दी। पंख फैलाकर उड़ जाने का मन मेरा भी था। मगर गुलामी में सीझी आत्मा के साथ मैं नितेश की आँखें आँजती रही। बेबी को गोद लिए मेघा नितेश को छेड़ती रही।
“देख ले भाई! तेरी बीवी को खाना बनवाने दिल्ली ले जाऊँगी।”
मुझे कसा-कसा देखकर वह बोली—“क्या हुआ कला भाभी? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तन को मन का साथी बनाने में थोड़ा समय लगता है। आगे से अपने आप को थोड़ा महत्त्व दोगी, तो एक साथ दोनों को पकड़ सकोगी।”
मेघा ने मेरी पीठ पर धौल जमाया। बिटिया को मेरी गोद में उतारते हुए कंधे मसक दिए। मैंने बेबी को अपने गाल से चिपकाया। लगा—ओस से भरा ठंडा फाहा किसी ने जलते गालों पर रख दिया हो। अच्छा लगा। आरामदायक।
“अपनी बेबी को मैं भी मेघा की तरह बनाऊँगी। खूब पढ़ाऊँगी। सही वक्त पर सही बात बोलना सिखाऊँगी।”
“कुछ कहा भाभी…?”
“नहीं… बेबी को…!”
झेंपकर मैंने मेघा को देखा। वह एक पोस्टर हाथ में लिए जा रही थी। पोस्टर पर—“नैना परिणय नितेश” लिखा था।
“मेघा, ये क्या किया? ये तो हमारी परंपरा के घोर विरुद्ध है। अपने यहाँ पुरुष का नाम ही आगे रहता है।” मैंने उसके कान में फुसफुसाया।
“नहीं भाभी! गौरी-शंकर… राधा-कृष्ण… सीता-राम!”
“अपनी परंपरा में स्त्री ही आगे रहती है। आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं—सुना भी नहीं।”
उसकी बड़ी-बड़ी मुस्कान से भरी आँखें चमक उठीं। जैसे पुरवाई का एक झोंका पूरे माहौल को थरथरा गया हो। मुझे तो अच्छा लगा लेकिन कई लोग आँचल में मुँह दबाकर प्रपंच करने लगे। भरे घर में चेहरों पर आते-जाते रंगों के बीच—मैं मेघा की खुशी अलग से देख पा रही थी।
मन में विचारों की लड़ियाँ छूट रही थीं। मेघा को देखकर पहली बार अपने भीतर रीढ़ महसूस हो रही थी। नितेश की टिकावन कर चाची ने बारात के लिए विदा कर दिया। बेबी के पापा मुझे नहीं दिखे। कहीं जाने की तैयारी में पहली बार उन्होंने मुझे नहीं पुकारा। यह उनकी गुस्सा थी या बदलाव—जानने की तमन्ना नहीं हुई।
बाहर-भीतर सब बारात जाने की प्रतीक्षा में थे। कुछ गाड़ियाँ निकल चुकी थीं। दूल्हे की गाड़ी और एक बस बाकी थी। इंदौर वाले फूफा का इंतज़ार हो रहा था। मैं अब भी दरवाज़े की ओर टकटकी लगाए थी—मेघा के लौट आने की आशंका समेटे। इतने में महराजिन हँसते हुए बोली—“बड़ी अम्मा! बरात कुसल से चली गई। मेघा बिटिया दूल्हे की कार में गई हैं।”
“क्या…?”
नए परिणय पोस्टर के साथ—जिसमें बहू का नाम आगे था… मैंने खुद से पूछा—और बेबी को चूम लिया।
कल्पना मनोरमा (जन्म : 4 जून 1972, इटावा, उत्तर प्रदेश) समकालीन हिंदी साहित्य की सशक्त रचनाकार हैं। उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी में स्नातकोत्तर तथा हिंदी में बी.एड. किया है। कविता, नवगीत, कहानी, बाल-साहित्य, निबंध, साक्षात्कार, संपादन और पत्रकारिता उनके लेखन के प्रमुख क्षेत्र हैं। दो दशकों तक अध्यापन के बाद वे शैक्षिक प्रकाशन संस्थानों में वरिष्ठ संपादक व हिंदी काउंसलर रहीं। उनकी प्रकाशित कृतियों में कब तक सूरजमुखी बनें हम, मौन के विरुद्ध, एक दिन का सफ़र आदि उल्लेखनीय हैं। उनके लेखन का केंद्र स्त्री-विमर्श, सामाजिक यथार्थ और मानवीय पीड़ा है।